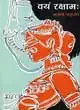|
बहुभागीय पुस्तकें >> सोना और खून - भाग 1 सोना और खून - भाग 1भोलानाथ तिवारी
|
305 पाठक हैं |
||||||
भारत में अंग्रेजी राज स्थापित होने की पूरी पृष्ठभूमि से आरंभ करके स्वतंत्रता प्राप्ति तक का संपूर्ण इतिहास...
इस पुस्तक का सेट खरीदें।
Sona Aur Khoon (1)
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
सोना पूँजी का प्रतीक है और खून युद्ध का। युद्ध प्रायः पूँजी के लिए होते हैं और पूँजी से ही लड़े जाते हैं। सोना और खून पूँजी के लिए लड़े जाने वाले एक महान युद्ध की विशाल पृष्ठभूमि पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है, आचार्य जी का सबसे बड़ा उपन्यास। इस उपन्यास के चार भाग है।
1.तूफान से पहले 2.तूफान 3.तूफान के बाद और 4.चिनगारियाँ। ये चारों भाग मुख्य कथा से सम्बद्ध होते हुए भी अपने में पूर्ण स्वतन्त्र है भारत में अंग्रेजी राज स्थापित होने की पूरी पृष्ठभूमि से आरम्भ होकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक का सारा इतिहास सरस कथा के माध्यम से इसमें आ गया है। इसमें आचार्य जी ने प्रतिपादित किया है कि भारत को अंग्रेजों ने नहीं जीता और 1857 की क्रांति राष्ट्रीय भावना पर आधारित नहीं थी। साथ ही वतन की स्वतन्त्रता प्राप्ति पर उस क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह उपन्यास एक अलग तरह की विशेषता लिए हुए हैं। इतिहास और कल्पना का ऐसा अद्भुत समन्वय आचार्यजी जैसे सिद्धहस्त कलाकार की लेखनी से ही सम्भव था।
1.तूफान से पहले 2.तूफान 3.तूफान के बाद और 4.चिनगारियाँ। ये चारों भाग मुख्य कथा से सम्बद्ध होते हुए भी अपने में पूर्ण स्वतन्त्र है भारत में अंग्रेजी राज स्थापित होने की पूरी पृष्ठभूमि से आरम्भ होकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक का सारा इतिहास सरस कथा के माध्यम से इसमें आ गया है। इसमें आचार्य जी ने प्रतिपादित किया है कि भारत को अंग्रेजों ने नहीं जीता और 1857 की क्रांति राष्ट्रीय भावना पर आधारित नहीं थी। साथ ही वतन की स्वतन्त्रता प्राप्ति पर उस क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह उपन्यास एक अलग तरह की विशेषता लिए हुए हैं। इतिहास और कल्पना का ऐसा अद्भुत समन्वय आचार्यजी जैसे सिद्धहस्त कलाकार की लेखनी से ही सम्भव था।
दो शब्द
सोना और खून का अर्थ है पूंजी और युद्ध। सोना और खून दस भागों और साठ खण्डों में कोई पांच हजार पृष्ठों का उपन्यास है। उसके प्रथम भाग के चार खण्ड आपके हाथ में हैं। प्रथम भाग के चार खण्डों में यूरोप की जन-क्रान्ति, पूंजीवाद और राष्ट्रवाद का विकास और भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के अमल के व्याख्यापूर्ण रेखाचित्र हैं। साथ ही जिस उद्योग-क्रान्ति से प्रेरित हो यूरोप, खास-कर इंग्लेंड विश्व का नेतृत्व करता जा रहा था, उसकी पृष्ठभूमि भी है। इस दृष्टिकोण को व्यक्त करने के अभिप्राय से मैंने कथा-प्रसंग को कहीं-कहीं उलटकर पीछे से लिखा है। इस उपन्यास में मेरी दृष्टि उपन्यास-तत्त्व की स्थापना करने की प्रमुख नहीं है। प्रमुख दृष्टि मध्यम श्रेणी के साधारण पढ़े-लिखे भारतीय जनों के समझ भारत से यूरोप के सम्पर्क, उसका भीतरी-बाहरी सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव वर्णन करना है। समूचे उपन्यास के साठ खण्डों में अंग्रेजों के भारत में आने और यहां से जाने तक के विवेचनात्मक इतिहास की पृष्ठभूमि में जन-क्रांति का इतिहास है, जो अन्यत्र प्रायः एकत्र मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के लिखने में मुझे बहुत-से ग्रन्थों का अध्ययन करना पड़ा है। पाठकों का ध्यान रखकर मैंने इसकी भाषा अधिकांश में सरल उर्दू मिश्रित रखी है। कहीं-कहीं आवश्यकता होने पर शुद्ध उर्दू ही रखी गई है। उपन्यास के इस प्रथम भाग के चारों खण्डों में मैंने तीन नकारों की स्थापना की व्याख्या की है :
1. क्या भारत को अंग्रेजों ने जीता ? नहीं।
2. क्या ’57 की क्रान्ति राष्ट्रीय भावना पर आधारित थी ? नहीं।
3. क्या वर्तमान स्वतन्त्रता-प्राप्त पर उस क्रान्ति का प्रभाव है ? नहीं।
निहसन्देह ये तीन नकार विचारणीय हैं। बहुत मनीषियों के विचारों से इनका मेल नहीं, परंतु मैं आशा करता हूं कि पाठक धैर्यपूर्वक मेरे इस उपन्यास में स्थापित आधारों का अध्ययन करेंगे।
उपन्यास में राष्ट्रवाद का उदय और उसका विश्व पर प्रभाव भी वर्णित है, वह भी मनन करने योग्य है।
दूसरे भाग के पाँचवें और छठे खण्डों में ’57 के विद्रोह का वर्णन और उसकी व्याख्या है।
उपन्यास के इस प्रथम भाग की तैयारी में मेरे दो मित्रों ने मुझे बहुत सहायता दी। एक निवाड़ी के कुअंर सुरेन्द्रपालसिंह त्यागी, दूसरे कविवर हंसराज रहबर। श्री त्यागी एक भावुक और विवेक तरुण हैं। नया ही मेरा उनसे परिचय हुआ है। पर यह पता नहीं चलता कि मैं उन्हें अधिक प्यार करता हूं या वे मुझे। उन्होंने मेरठ, मुजफ्फर नगर, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ के बहुत से तथ्य मुझे दिए, जिन पर मैं अपनी कल्पना की तूलिका चला सका। श्री रहबर एक दिलफेंक साहित्यकार हैं।
विधाता ने गलती से बीवी-बच्चों को इस फक्कड़ साहित्य-शिल्पी के पल्ले बांध दिया। ऐसा लगता है कि वे हिन्दी के प्रेमी और उर्दू के शिल्पी हैं। हिन्दी का उनका आचरण बड़ा अटपटा है। उसमें बच्चों की तुतलाहट का मज़ा आता है। मैं बदनसीब उर्दू पढ़ नहीं सकता, श्री रहबर घण्टों मेरे पास बैठकर ’57 से सम्बन्धित संदर्भ उर्दू से छांट-छांट कर लाते और सुनाते तथा नोट कराते हैं। सच पूछिए तो इन दोनों मित्रों की पूंजी पर ही प्रथम भाग का सारा कारोबार चला है।
मेरे परम मित्र दिल्ली के नामांकित चिकित्सक पण्डित परमानन्द वैद्यरत्न का आभार यदि मैं न स्वीकार करूँ तो कृतघ्नता होगी। गत दो वर्षों से मैं अस्वस्थ ही चल रहा हूं। और इस अस्वस्थता में मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं। यह सोना और खून, कदाचित आपके सम्मुख इतने शीघ्र न आ पाती यदि वैद्यरत्न जी सोना मेरे खून में प्रविष्ट न करते।
अब आप इस प्रथम भाग को पढ़िए और मैं दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की चेष्टा करूं।
1. क्या भारत को अंग्रेजों ने जीता ? नहीं।
2. क्या ’57 की क्रान्ति राष्ट्रीय भावना पर आधारित थी ? नहीं।
3. क्या वर्तमान स्वतन्त्रता-प्राप्त पर उस क्रान्ति का प्रभाव है ? नहीं।
निहसन्देह ये तीन नकार विचारणीय हैं। बहुत मनीषियों के विचारों से इनका मेल नहीं, परंतु मैं आशा करता हूं कि पाठक धैर्यपूर्वक मेरे इस उपन्यास में स्थापित आधारों का अध्ययन करेंगे।
उपन्यास में राष्ट्रवाद का उदय और उसका विश्व पर प्रभाव भी वर्णित है, वह भी मनन करने योग्य है।
दूसरे भाग के पाँचवें और छठे खण्डों में ’57 के विद्रोह का वर्णन और उसकी व्याख्या है।
उपन्यास के इस प्रथम भाग की तैयारी में मेरे दो मित्रों ने मुझे बहुत सहायता दी। एक निवाड़ी के कुअंर सुरेन्द्रपालसिंह त्यागी, दूसरे कविवर हंसराज रहबर। श्री त्यागी एक भावुक और विवेक तरुण हैं। नया ही मेरा उनसे परिचय हुआ है। पर यह पता नहीं चलता कि मैं उन्हें अधिक प्यार करता हूं या वे मुझे। उन्होंने मेरठ, मुजफ्फर नगर, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ के बहुत से तथ्य मुझे दिए, जिन पर मैं अपनी कल्पना की तूलिका चला सका। श्री रहबर एक दिलफेंक साहित्यकार हैं।
विधाता ने गलती से बीवी-बच्चों को इस फक्कड़ साहित्य-शिल्पी के पल्ले बांध दिया। ऐसा लगता है कि वे हिन्दी के प्रेमी और उर्दू के शिल्पी हैं। हिन्दी का उनका आचरण बड़ा अटपटा है। उसमें बच्चों की तुतलाहट का मज़ा आता है। मैं बदनसीब उर्दू पढ़ नहीं सकता, श्री रहबर घण्टों मेरे पास बैठकर ’57 से सम्बन्धित संदर्भ उर्दू से छांट-छांट कर लाते और सुनाते तथा नोट कराते हैं। सच पूछिए तो इन दोनों मित्रों की पूंजी पर ही प्रथम भाग का सारा कारोबार चला है।
मेरे परम मित्र दिल्ली के नामांकित चिकित्सक पण्डित परमानन्द वैद्यरत्न का आभार यदि मैं न स्वीकार करूँ तो कृतघ्नता होगी। गत दो वर्षों से मैं अस्वस्थ ही चल रहा हूं। और इस अस्वस्थता में मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं। यह सोना और खून, कदाचित आपके सम्मुख इतने शीघ्र न आ पाती यदि वैद्यरत्न जी सोना मेरे खून में प्रविष्ट न करते।
अब आप इस प्रथम भाग को पढ़िए और मैं दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की चेष्टा करूं।
-चतुरसेन
सोना और खून
सोने का रंग पीला होता है और खून का रंग सुर्ख। पर तासीर दोनों की एक है। खून मनुष्य की रगों में बहता है, और सोना उसके ऊपर लदा हुआ है। खून मनुष्य को जीवन देता है, और सोना उसके जीवन पर खतरा लाता है। पर आज के मनुष्य का खून पर मोह नहीं है, सोने पर है। वह एक-एक रत्ती सोने के लिए अपने शरीर का एक-एक बूंद खून बहाने को आमादा है। जीवन को सजाने के लिए वह सोना चाहता है, और उसके लिए खून बहाकर वह जीवन को खतरे में डालता है। आज के सभ्य संसार का यह सबसे बड़ा कारोबार है। सबसे बड़े लेन-देन है खून देना और सोना लेना।
सोना और खून के इस लेन-देन ने आज मनुष्य को ही मनुष्य का सबसे बड़ा खतरा बना दिया है। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह बुद्धिमान् है। सोना और खून के इस कारोबार ने उसके सारे बुद्धिबल को उसके अपने ही विनाश में लगा दिया है; और अब विनाश ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। ज़िन्दा रहने की उसकी सारी चेष्टाएं अब हास्यास्पद हो गई हैं। वह मनुष्य का बोझ अपने कंधों पर लादे हुए थकावट से चूर-चूर, पसीने से लथपथ, विश्राम की खोज में भटक रहा है। और मौत उसे कह रही है—यहां आ, और मेरी गोद में विश्राम कर।
सुधारक लोग सपने देखते हैं कि ज्ञान और सदाचार मनुष्य के दुःख-दर्द हर लेंगे। मनुष्य का जीवन सफल होगा। जेलखाने ढहा दिए जाएंगे। फांसी के तख्ते दुनिया से उठा दिए जाएंगे। जेल की काल-कोठरियां प्रकाश से जगमगा उठेंगी। कोई दरिद्र न रहेगा। कोई भीख के लिए हाथ पसारता नज़र न आएगा। सारे मनुष्य समझदार, सदाचारी और सुखी हो जाएंगे, किन्तु कब ? ये सपने तो उन्होंने युग-युग से देखे हैं, और युग-युग तक देखते रहेंगे।
असभ्य युग का आदमी भी मन का कमजोर, भीरु और आलसी था। वह जो देखता था, उसे ही समझता था। विपत्ति पड़ने पर प्रकृति से परे किसी अदृष्ट शक्ति को खोजता था। सहस्राब्दियों तक वह बलिदानों, प्रार्थनाओं और अलौकिक पूजाओं से उसकी उपासना करता रहा। बहुत धीरे-धीरे बड़े कष्ट से उसकी विचार-सत्ता विकसित हुई। मन शरीर का सहायक बना, विचार और परिश्रम एकत्र हुए, मनुष्य की उन्नति का सूत्रपात हुआ, कि उसे सोना मिल गया। उसने तत्काल ही खून से सोने का लेन-देन आरम्भ कर दिया। और देखते ही देखते वह घनघोर युद्धों के बीच में जा फंसा, जिन्होंने उसे कर्जदार, दिवालिया और असहाय बना दिया।
इस नये युग का नया खूनी देवता है—देश। इस देवता ने इस सभ्य युग में जन्म लेकर दुनिया के सब देवताओं को पीछे धकेल दिया। आज वह संसार के मनुष्य का सबसे बड़ा देवता है। असभ्य युग में, असभ्य जातियों में कभी भी किसी देवता को इतनी नरबलि न दी थी, जितनी इस युग में इस खूनी और हत्यारे देवता को मनुष्य ने दी है, और देता जा रहा है। भयानक देवता की खून की प्यास का अन्त नहीं है। बलिदान की पुरानी तलवार के स्थान पर मनुष्य ने अपना सारा बुद्धिबल खर्च करके एक से एक बढ़कर खूनी हथियार इस देवता को नरबलि से संतुष्ट करने के लिए बनाए हैं। रोज़ मनुष्य का ताज़ा रक्त इस देवता को चाहिए। जो सबसे अधिक नर-वध कर सकता है, वही सबसे अधिक इस देवता का वरदान प्राप्त कर सकता है। यह हत्यारा देवता शायद संसार के सारे नृवंश को खा जाएगा। एक भी आदमी के बच्चे को जीता नहीं छोड़ेगा।
यह खूनी देवता यूरोप में उत्पन्न हुआ, और वहां से अंग्रेज उसे भारत में अपने साथ लाए। पाश्चात्य संस्कृति ने इस देवता को जन्म दिया था। उसकी नींव ग्रीकों ने डाली थी। मिस्र और बेबीलोनिया के प्राचीन साम्राज्यों के नष्ट होने पर जब ग्रीकों का उदय हुआ, तो उसमें सर्वप्रथम सार्वभौम राजा की पूजा खत्म कर दी गई। इससे वहां के मध्यमवर्ग के अधिकार बहुत बढ़ गए और कला-कौशल और तत्त्व-ज्ञान में वे अपने काल की सब जातियों से बढ़ गए। रोमन विजेताओं ने ग्रीक दासों से ही कला-कौशल और तत्त्व-ज्ञान सीखे। बाद में रोमन प्रजातन्त्र का उदय हुआ, और उसके बाद यूरोप में ईसाई धर्म का उदय हुआ, और साम्राज्य का नेता पोप बन बैठा। शताब्दियों तक सारे यूरोप की राजसत्ताएं उसके हाथ की कठपुतलियां बनी रहीं। यह यूरोप की अन्धाधुन्धी का मध्ययुग था। उसी समय यूरोप पर मंगोलों ने आक्रमण किया और उसके बाद ही तुर्कों ने समूचे पूर्वी यूरोप को ग्रस लिया। परन्तु यूरोप का विकास तेरहवीं शताब्दी से ही होने लगा था। वेनिस, जेनेवा, पीसा, फ्लोरेंस आदि नगरों का उदय हो चुका था, जिनका पोषण व्यापार से होता था। उस समय सारे व्यापार का केन्द्र-मार्ग कुस्तुनिया होकर था। भारत और चीन के सम्बन्ध में उस समय भी यूरोप के लोग कुछ नहीं जानते थे।
परन्तु जब भूमध्यसागर और अटलांटिक महासागर की छाती पर सवार होकर पोर्चुगीज नाविक दीयाज़, कोलम्बस, वास्को-द-गामा के ऐतिहासिक अभियान हुए तो, पूर्व का द्वार यूरोप के लिए खुल गया। भारत, चीन और अमरीका की उन्हें उपलब्धि हुई। और इन देशों की सम्पत्ति पर सारे पश्चिम यूरोप की लोलुप दृष्टि पड़ी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। पोर्चुगीज़ों के बाद डच और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उद्योग किए। फ्रेंचो ने भी हांथ-पैर मारे। अन्त में प्लासी के निर्णायक युद्ध में अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में पड़ी। आज इस राजा का और कल उस नवाब का पक्ष लेकर, उन्होंने अन्ततः सारा भारत अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने रजवाड़ों को हड़पने की चेष्टा की, जिसके फलस्वरूप सत्तावन का विद्रोह उठ खड़ा हुआ। जिसमें फांसी पर चढ़ाकर और तोप के मुंह पर बांध जीवित मनुष्यों को उड़ाकर नर-वध का महाताण्डव करके अंग्रेज़ भारत के एकनिष्ठ अधिराज बन बैठे।
भारत में पोर्चुगीज, डच और फ्रेंचों के मुकाबले में अंग्रेजों को जो सफलता मिली, वह केवल अंग्रेज़ों के भाग्योदय के कारण नहीं। इसका कारण वह औद्योगिक क्रान्ति थी, जिसका श्रीगणेश यूरोप में पन्द्रहवीं शताब्दी में ही हो गया था। इसके अतिरिक्त अपनी कूटनीति और उद्योगों से, अंग्रेज़ सब यूरोपियन देशों से बाज़ी मार ले गए। इस समय अंग्रेज़ सरदारों और मध्यमवर्ग के लोगों ने जो राजा पर अंकुश लगाकर पार्लियामेंट की स्थापना कर ली थी, उससे इस औद्योगिक क्रान्ति के पर लग गए थे। इसके बाद सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड ने मार्टिन लूथर का पंथ स्वीकार कर पोप के धार्मिक प्रभुत्व का अन्त कर दिया। सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैंड के मध्यमवर्ग में और भी जागृति हुई।
बढ़ते हुए मध्यमवर्ग ने अपनी बात पर आड़ लगाने के अपराध में अपने बादशाह चार्स्स का सिर काट लिया। उनके नेता दृढ़ निश्चयी क्रामवेल के सामने यूरोप-भर के राजाओं ने विद्रोह किया पर बेकार। इसके बाद तो राजा के अधिकार कम होते ही गए और मध्यमवर्ग पनपता गया। फिर भी अंग्रेजों ने प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं की, क्योंकि उसका जाल यूरोप के दूसरे देशों में फैल गया था। इन देशों के राजाओं से पत्र-व्यवहार करने और विजित देशों पर निरंकुश शासन की आड़ में निर्द्वन्द्व होकर उनका लहू चूसने के लिए ‘राजा’ नामक एक खिलौने की उन्हें बड़ी आवश्यकता थी। इसी से उन्होंने अपनी राजसत्ता को कायम रखा। जब कभी पार्लियामेंट गलती करके कोई संकट खड़ा कर देती, तो यह खिलौना राजा उससे बच निकलने में अंग्रेजों की मदद करता था। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी यह जातीय नीति बना ली कि चाहे राजसत्ता हो या धर्मसत्ता, जब उससे लाभ उठाने का अवसर मिले लाभ उठा लेना जब वह राह का रोड़ा बने, उसे ठोकर लगा देना। अंग्रेज़ों की यह नीति भारत में ही नहीं यूरोप के अन्य देशों के मध्यम वर्ग पर विजय में भी बड़ी सहायक हुई।
सोना और खून के इस लेन-देन ने आज मनुष्य को ही मनुष्य का सबसे बड़ा खतरा बना दिया है। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह बुद्धिमान् है। सोना और खून के इस कारोबार ने उसके सारे बुद्धिबल को उसके अपने ही विनाश में लगा दिया है; और अब विनाश ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। ज़िन्दा रहने की उसकी सारी चेष्टाएं अब हास्यास्पद हो गई हैं। वह मनुष्य का बोझ अपने कंधों पर लादे हुए थकावट से चूर-चूर, पसीने से लथपथ, विश्राम की खोज में भटक रहा है। और मौत उसे कह रही है—यहां आ, और मेरी गोद में विश्राम कर।
सुधारक लोग सपने देखते हैं कि ज्ञान और सदाचार मनुष्य के दुःख-दर्द हर लेंगे। मनुष्य का जीवन सफल होगा। जेलखाने ढहा दिए जाएंगे। फांसी के तख्ते दुनिया से उठा दिए जाएंगे। जेल की काल-कोठरियां प्रकाश से जगमगा उठेंगी। कोई दरिद्र न रहेगा। कोई भीख के लिए हाथ पसारता नज़र न आएगा। सारे मनुष्य समझदार, सदाचारी और सुखी हो जाएंगे, किन्तु कब ? ये सपने तो उन्होंने युग-युग से देखे हैं, और युग-युग तक देखते रहेंगे।
असभ्य युग का आदमी भी मन का कमजोर, भीरु और आलसी था। वह जो देखता था, उसे ही समझता था। विपत्ति पड़ने पर प्रकृति से परे किसी अदृष्ट शक्ति को खोजता था। सहस्राब्दियों तक वह बलिदानों, प्रार्थनाओं और अलौकिक पूजाओं से उसकी उपासना करता रहा। बहुत धीरे-धीरे बड़े कष्ट से उसकी विचार-सत्ता विकसित हुई। मन शरीर का सहायक बना, विचार और परिश्रम एकत्र हुए, मनुष्य की उन्नति का सूत्रपात हुआ, कि उसे सोना मिल गया। उसने तत्काल ही खून से सोने का लेन-देन आरम्भ कर दिया। और देखते ही देखते वह घनघोर युद्धों के बीच में जा फंसा, जिन्होंने उसे कर्जदार, दिवालिया और असहाय बना दिया।
इस नये युग का नया खूनी देवता है—देश। इस देवता ने इस सभ्य युग में जन्म लेकर दुनिया के सब देवताओं को पीछे धकेल दिया। आज वह संसार के मनुष्य का सबसे बड़ा देवता है। असभ्य युग में, असभ्य जातियों में कभी भी किसी देवता को इतनी नरबलि न दी थी, जितनी इस युग में इस खूनी और हत्यारे देवता को मनुष्य ने दी है, और देता जा रहा है। भयानक देवता की खून की प्यास का अन्त नहीं है। बलिदान की पुरानी तलवार के स्थान पर मनुष्य ने अपना सारा बुद्धिबल खर्च करके एक से एक बढ़कर खूनी हथियार इस देवता को नरबलि से संतुष्ट करने के लिए बनाए हैं। रोज़ मनुष्य का ताज़ा रक्त इस देवता को चाहिए। जो सबसे अधिक नर-वध कर सकता है, वही सबसे अधिक इस देवता का वरदान प्राप्त कर सकता है। यह हत्यारा देवता शायद संसार के सारे नृवंश को खा जाएगा। एक भी आदमी के बच्चे को जीता नहीं छोड़ेगा।
यह खूनी देवता यूरोप में उत्पन्न हुआ, और वहां से अंग्रेज उसे भारत में अपने साथ लाए। पाश्चात्य संस्कृति ने इस देवता को जन्म दिया था। उसकी नींव ग्रीकों ने डाली थी। मिस्र और बेबीलोनिया के प्राचीन साम्राज्यों के नष्ट होने पर जब ग्रीकों का उदय हुआ, तो उसमें सर्वप्रथम सार्वभौम राजा की पूजा खत्म कर दी गई। इससे वहां के मध्यमवर्ग के अधिकार बहुत बढ़ गए और कला-कौशल और तत्त्व-ज्ञान में वे अपने काल की सब जातियों से बढ़ गए। रोमन विजेताओं ने ग्रीक दासों से ही कला-कौशल और तत्त्व-ज्ञान सीखे। बाद में रोमन प्रजातन्त्र का उदय हुआ, और उसके बाद यूरोप में ईसाई धर्म का उदय हुआ, और साम्राज्य का नेता पोप बन बैठा। शताब्दियों तक सारे यूरोप की राजसत्ताएं उसके हाथ की कठपुतलियां बनी रहीं। यह यूरोप की अन्धाधुन्धी का मध्ययुग था। उसी समय यूरोप पर मंगोलों ने आक्रमण किया और उसके बाद ही तुर्कों ने समूचे पूर्वी यूरोप को ग्रस लिया। परन्तु यूरोप का विकास तेरहवीं शताब्दी से ही होने लगा था। वेनिस, जेनेवा, पीसा, फ्लोरेंस आदि नगरों का उदय हो चुका था, जिनका पोषण व्यापार से होता था। उस समय सारे व्यापार का केन्द्र-मार्ग कुस्तुनिया होकर था। भारत और चीन के सम्बन्ध में उस समय भी यूरोप के लोग कुछ नहीं जानते थे।
परन्तु जब भूमध्यसागर और अटलांटिक महासागर की छाती पर सवार होकर पोर्चुगीज नाविक दीयाज़, कोलम्बस, वास्को-द-गामा के ऐतिहासिक अभियान हुए तो, पूर्व का द्वार यूरोप के लिए खुल गया। भारत, चीन और अमरीका की उन्हें उपलब्धि हुई। और इन देशों की सम्पत्ति पर सारे पश्चिम यूरोप की लोलुप दृष्टि पड़ी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। पोर्चुगीज़ों के बाद डच और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उद्योग किए। फ्रेंचो ने भी हांथ-पैर मारे। अन्त में प्लासी के निर्णायक युद्ध में अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में पड़ी। आज इस राजा का और कल उस नवाब का पक्ष लेकर, उन्होंने अन्ततः सारा भारत अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने रजवाड़ों को हड़पने की चेष्टा की, जिसके फलस्वरूप सत्तावन का विद्रोह उठ खड़ा हुआ। जिसमें फांसी पर चढ़ाकर और तोप के मुंह पर बांध जीवित मनुष्यों को उड़ाकर नर-वध का महाताण्डव करके अंग्रेज़ भारत के एकनिष्ठ अधिराज बन बैठे।
भारत में पोर्चुगीज, डच और फ्रेंचों के मुकाबले में अंग्रेजों को जो सफलता मिली, वह केवल अंग्रेज़ों के भाग्योदय के कारण नहीं। इसका कारण वह औद्योगिक क्रान्ति थी, जिसका श्रीगणेश यूरोप में पन्द्रहवीं शताब्दी में ही हो गया था। इसके अतिरिक्त अपनी कूटनीति और उद्योगों से, अंग्रेज़ सब यूरोपियन देशों से बाज़ी मार ले गए। इस समय अंग्रेज़ सरदारों और मध्यमवर्ग के लोगों ने जो राजा पर अंकुश लगाकर पार्लियामेंट की स्थापना कर ली थी, उससे इस औद्योगिक क्रान्ति के पर लग गए थे। इसके बाद सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड ने मार्टिन लूथर का पंथ स्वीकार कर पोप के धार्मिक प्रभुत्व का अन्त कर दिया। सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैंड के मध्यमवर्ग में और भी जागृति हुई।
बढ़ते हुए मध्यमवर्ग ने अपनी बात पर आड़ लगाने के अपराध में अपने बादशाह चार्स्स का सिर काट लिया। उनके नेता दृढ़ निश्चयी क्रामवेल के सामने यूरोप-भर के राजाओं ने विद्रोह किया पर बेकार। इसके बाद तो राजा के अधिकार कम होते ही गए और मध्यमवर्ग पनपता गया। फिर भी अंग्रेजों ने प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं की, क्योंकि उसका जाल यूरोप के दूसरे देशों में फैल गया था। इन देशों के राजाओं से पत्र-व्यवहार करने और विजित देशों पर निरंकुश शासन की आड़ में निर्द्वन्द्व होकर उनका लहू चूसने के लिए ‘राजा’ नामक एक खिलौने की उन्हें बड़ी आवश्यकता थी। इसी से उन्होंने अपनी राजसत्ता को कायम रखा। जब कभी पार्लियामेंट गलती करके कोई संकट खड़ा कर देती, तो यह खिलौना राजा उससे बच निकलने में अंग्रेजों की मदद करता था। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी यह जातीय नीति बना ली कि चाहे राजसत्ता हो या धर्मसत्ता, जब उससे लाभ उठाने का अवसर मिले लाभ उठा लेना जब वह राह का रोड़ा बने, उसे ठोकर लगा देना। अंग्रेज़ों की यह नीति भारत में ही नहीं यूरोप के अन्य देशों के मध्यम वर्ग पर विजय में भी बड़ी सहायक हुई।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book